साधारण अपवाद: बाल्यपन, पागलपन, मत्तता-part 4.2
साधारण अपवाद वाले आईपीसी से अध्याय 4 में जिन 12 प्रकार के अपवादों का उल्लेख है उनमें बाल्यपन, पागलपन और मत्तता भी आते हैं। क्योंकि इस स्थिति में आपराधिक कार्य करने वाले का कोई आपराधिक आशय नहीं होता है।
बाल्यपन (infancy) (धारा 82-83)
धारा 82- सात वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य- कोई बात अपराध नहीं है, जो सात वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है।
धारा 83- सात वर्ष से ऊपर किन्तु बारह वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य- कोई बात अपराध नहीं है, जो सात वर्ष से ऊपर और बारह वर्ष से कम आयु के ऐसे शिशु द्वारा की जाती है जिसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं हुई है कि वह उस अवसर पर अपने आचरण की प्रकृति और परिणामों का निर्णय कर सके।
पागलपन (insanity) (धारा 84)
84. विकृतचित्त व्यक्ति का कार्य- कोई बात अपराध नहीं है, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है, जो उसे करते समय चित्तविकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति, या यह कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ है।
धारा 84 के साधारण अपवाद का बचाव लेने के लिए इन अवयवों की उपस्थिति अनिवार्य है–
(1) अभियुक्त अस्वस्थ मस्तिष्क का हो;
(2) वह समझने में असमर्थ हो कि:
. (1) उस कार्य की प्रकृति क्या है, अर्थात् वह अनुचित है, या
(2) उसका कार्य विधि विरूद्ध है, या
(3) उसका कार्य दोषपूर्ण है।
(3) ऐसी अक्षमता अपराधी के अस्वस्थ मस्तिष्क के कारण हो
मस्तिष्क की विधिक अक्षमता चिकित्सीय अक्षमता से भिन्न होता है। अभियुक्त यदि जानता है कि उसका कार्य अनुचित है तब उसे अपवाद का लाभ नहीं मिलेगा भले ही वह यह जानता हो या नहीं कि वह कार्य विधि विरूद्ध है।
दूसरी आवश्यकता यह है कि चित्तविकृति अपराध करते समय होना चाहिए। चित्तविकृति को सिद्ध करने का दायित्व अभियुक्त पर है। लेकिन उसे ‘संदेहों से परे‘ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है कि वह चित्तविकृत था और इस कारण कार्य की प्रकृति समझने में असमर्थ था। (सुरजू मारन्डे बनाम बिहार राज्य (1977 Cri LJ 1765)
Case Laws
मैक्नाटेन केस (Mc Naghten case) (R v Mc Naghten) (1843 8 ER718, Volume 8; (1843) 10 Cl. & F.)
मैक्नाटेन को विभ्रम की बीमारी थी। उसे यह भ्रम हो गया था कि इंग्लैण्ड के तत्कालिन प्रधानमंत्री सर राबर्ट पील उसे क्षति पहुँचाना चाहते है। इस कारण वह उन्हें मारना चाहता था। लेकिन भूल से उसने पील समझ कर उनके वैयक्तिक सचिव एडमण्ड ड्रमण्ड पर गोली चला दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई।
मैक्नाटेन ने अपने बचाव में पागलपन का अभिवचन किया और चिकित्सीय प्रमाणों से यह दर्शाया कि वह विकृत भ्रम से पीड़ित था जिसके कारण वह नियंत्रण नहीं कर पाया। इस आधार पर उसे आरोपों से बरी कर दिया गया।
उसको बरी करने की आलोचना हुई और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में यह विवाद का विषय बन गया। अतंतः हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने विक्षिप्तता के मामलों में आपराधिक दायित्व सम्बन्धी सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए यह मामला 15 न्यायाधीशों की एक पीठ को सौंप दिया। इस पीठ ने इस मामलें जो प्रेक्षण किया वह मैक्नाटेन के नियम कहे जाते हैं ओर विक्षिप्तता से संबंधित आधुनिक विधि के आधार हैं। इसके प्रमुख सिद्धांत या नियम निम्नलिखित हैं–
(1) भले ही अभियुक्त चित्तविकृति के प्रभाववश कोई कार्य करे लेकिन यदि वह ऐसे अपराध को कारित करते समय यह जानता था कि सका कार्य विधि विरूद्ध है तो वह कारित कार्य की प्रकृति के अनुसार दण्डनीय है।
(2) सामान्य संकल्पना यह है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ मस्तिष्क का होता है और अपने कार्यों की प्रकृति को भली भाँति जानता है। अगर तथ्य इसके विपरीत है तो यह अभियुक्त को विशेष रूप से अभिवाक् करना होगा और इसे साबित करना होगा।
(3) चित्तविकृति के आधार पर बचाव सिद्ध करने के लिए यह स्पष्टतः स्थापित होना चाहिए कि वह कार्य करते समय अभियुक्त मस्तिष्कीय रोग के कारण ऐसे दोष से पीड़ित था कि वह अपने द्वारा किए हुए कार्य की प्रकृति तथा उसके औचित्य को समझने के असमर्थ था या यदि वह इसे नहीं जानता था, तो वह यह भी नहीं जानता था कि जो कुछ वह कर रहा है वह विधिविरूद्ध है। लेकिन यदि वह जानता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए तो वह दण्डनीय होगा।
(4) यदि अभियुक्त मात्र आंशिक भ्रांति से प्रभावित है और अन्य संदर्भों में वह विकृतचित्त नहीं है तो उत्तरदायित्व हेतु उसे उसी स्थिति में माना जाना चाहिए कि वे तथ्य जिनके सम्बन्धों में भ्रांति अस्तित्ववान है, सचमुच यथार्थ है।
उदाहरण के लिये, यदि इस भाँति के प्रभाव के अन्तर्गत यह सोचता है कि एक दूसरा व्यक्ति उसे मारने का प्रयास कर रहा है और वह उस व्यक्ति को मार डालता है और ऐसा वह आत्मरक्षा के लिए करता है तो वह दण्ड से उन्मुक्त होगा। लेकिन यदि उसका भ्रम यह है कि मृतक ने उसके चरित्र तथा उसकी सम्पदा पर घातक प्रहार किया हे और उसने मृतक को इसके प्रतिशोध में मार डाला तो वह दण्डित किया जायेगा।
(5) एक चिकित्सक, जो कि चित्तविकृतता के रोग का ज्ञाता है और जिसने अभियुक्त को विचारण के पूर्व कभी नहीं देखा था, किंतु जो अभियुक्त के सम्पूर्ण विचारण तथा परीक्षण के दौरान विद्यमान था, से उसकी राय अपराध कारित करते समय अभियुक्त की मस्तिष्क की स्थिति के बारे में नहीं मांगी जाएगी बल्कि यह तथ्य जूरी द्वारा विनिश्चित किया जाएगा।
मत्तता (intoxication) (धारा 85, 86)
85. ऐसे व्यक्ति के कार्य जो अपनी इच्छा के विरूद्ध मत्तता में होने के कारण निर्णय पर पहुँचने में असमर्थ है- कोई बात अपराध नहीं है,जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है, जो उसे करते समय मत्तता के कारण उस कार्य की प्रकृति, या यह कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ है, परन्तु यह तब जबकि वह चीज, जिससे उसकी मत्तता हुई थी, उसके अपने ज्ञान के बिना या इच्छा के विरूद्ध दी गई थी।
86. किसी व्यक्ति द्वारा, जो मत्तता में है किया गया अपराध जिसमें विशेष आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है- उन दशाओं में, जहाँ कि कोई किया गया कार्य अपराध नहीं होता जब तक कि वह किसी विशिष्ट ज्ञान या आशय से न किया गया हो, कोई व्यक्ति जो वह कार्य मत्तता की हालत में करता है, इस प्रकार बरते जाने के दायित्व के अधीन होगा मानो उसे वही ज्ञान था जो उसे होता यदि वह मत्तता में न होता जब तक कि वह चीज, जिससे उसे मत्तता हुई थी, उसे उसके ज्ञान के बिना या उसकी इच्छा के विरूद्ध न दी गई हो।
साधारण अपवाद के रूप में धारा 85 का बचाव लेने के लिए इन अवयवों की उपस्थित सिद्ध करना आवश्यक है-
1. कार्य करते समय मत्तता के कारण यह समझने में असमर्थ था कि–
(1) उसके कार्य की प्रकृति क्या है अर्थात् कार्य अनुचित है, या
(2) उसका कार्य दोषपूर्ण और विधि विरूद्ध है
2. जिस वस्तु ने उसे उन्मत किया था, वह
(1) उसके ज्ञान के बिना उसे दी गई थी, अथवा
(2) उसकी इच्छा के विरूद्ध उसे दी गई हो।
धारा 85 अनैच्छिक मत्तता से संबंधित प्रावधान करती है। यह धारा अभियुक्त को वही बचाव प्रदान करती है जो धारा 84 एक अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति को प्रदान करती है।
धारा 86
इस धारा में स्वैच्छिक मत्तता से संबंधित प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से मत्त हुआ है तो यह माना जाएगा कि उसे वही ज्ञान था जो उसे रहा होता यदि वह मत्त नहीं हुआ होता। यह धारा मत्त व्यक्ति को एक सामान्य प्रज्ञा वाले व्यक्ति के ज्ञान से युक्त मानती है किन्तु उसे सामान्य प्रज्ञा वाले व्यक्ति के आशय से युक्त नहीं मानती।
एक सामान्य व्यक्ति से अपेक्षा किया जाता है कि वह अपने कृत्य के स्वभाविक परिणामो को जानता है, इसलिए यदि वह जानता है कि उसके कार्य का स्वभाविक परिणाम क्या है तो यह माना जाएगा कि उसका वही आशय था। किंतु ज्ञान से आशय का यह निष्कर्ष उस समय उत्पन्न नहीं होगा जब वह मत्त था।
एच्छिक मत्तता धारा 86 के अन्तर्गत उन मामलों में कोई बचाव नहीं प्रदान करती जिसमें अपराध गठित करने के लिए मात्र आवश्यक ज्ञान का अभाव था यद्यपि इसका प्रयोग यह दिखाने में किया जा सकता है कि यदि किसी आशय की आवश्यकता थी तो वह अनुपस्थित था। अर्थात् उसे केवल ज्ञान के आधार पर दण्डित किया जा सकता है किसी विशिष्ट आशय के आधार पर नहीं।
धारा 86 के मुख्य अवयव हैं अर्थात अगर ये तत्त्व उपस्थित होंगे तो वह कार्य आपराधिक दायित्व से मुक्ति के लिए साधारण अपवाद में आ जाएगा–
1. उस कार्य को अपराध बनाने के लिए ज्ञान या आशय आवश्यक हो;
2. जिस चीज से मत्तता हुई थी, वह उसने स्वैच्छिक रूप से लिया हो तो माना जाएगा कि उसे वही ज्ञान था जो उसे तब होता यदि वह मत्तता में न होता।
मत्त यानि कि नशे में होना आपराधिक कृत्य के दायित्व से मुक्त नहीं करता। इस सामान्य नियम के दो अपवाद हैं–
1. लगातार नशा के कारण मस्तिष्क में कोई स्थायी विकृति आ गई हो, जैसे– डिलीरियम ट्रीमेंस (delirium tremens), मादक पागलपन (alcoholic dementia) आदि बीमारी।
2. जिस चीज के नशा हुई है, वह ज्ञान या इच्छा के विरूद्ध ली गई हो।
डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोजीक्यूशन बनाम बियर्ड (1920 AC 479)
अभियुक्त पर एक तेरह वर्षीया लड़की के साथ बलात्कार के प्रयास और हत्या का अभियोग था। अभियुक्त, जो कि एक मिल में पहरेदार के रूप में कार्यरत था, ने मिल के फाटक से गुजरते हुए उस लड़की के बलात्कार का प्रयत्न किया। लड़की जब प्रतिरोध करने लगी तो अपना हाथ लड़की के मुँह पर रख दिया और दूसरे हाथ के अँगूठे से उसका गला दबाया ताकि वह शोर न कर सके। लड़की की मृत्यु हो गई।
अभियुक्त ने मत्तता का प्रतिरक्षा लिया। उसका पक्ष था कि मत्तता के कारण वह अपने कार्य की प्रकृति नहीं समझ सका था और न ही मृत्यु कारित करने का उसका आशय था। कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील ने उसे आपराधिक मानव वध का दोषी पाया किन्तु हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने उसे हत्या के लिए दोषी पाया और मृत्युदण्ड दिया।
यह पाया गया कि भले ही उसका आशय मृत्यु कारित करना नहीं हो लेकिन उसके कार्य से यह स्पष्ट है कि वह यह जानता था कि उसके कार्य की प्रकृति क्या है लड़की को शोर करने से रोकना इसका प्रमाण है। इस मामले में निम्नलिखित महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किये गये–
(1) जहाँ आशय अपराध के लिए आवश्यक तत्व है वहाँ मत्तता के कारण यदि वह आशय सृजित करने में असक्षम है तो इस अपराध के लिए उसे दण्डित नहीं किया जाएगा। किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उसे दण्डित नहीं किया जाएगा और मत्तता स्वयं में उन्मुक्ति है। उसे उसके ज्ञान के आधार पर दण्डित किया जाएगा।
(2) चित्तविकृति आरोपित अपराध के लिए बचाव है भले ही वह अत्यधिक मदिरापान से उत्पन्न हुआ हो। विधि चित्तविकृति के कारण पर ध्यान नहीं देती। चित्तविकृति आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति देती है भले ही वह अस्थायी ही क्यों न हो।
जहाँ साक्ष्य से यह सिद्ध हो गया कि अभियुक्त का मस्तिष्क अस्वस्थ था तथा वह डिलीरियम ट्रीमेंस से पीड़ित था और यह अत्यधिक मदिरापान से उत्पन्न हुआ था, ऐसी स्थिति में यह निर्णय दिया गया कि ‘‘मदिरापान एक चीज है तथा मदिरापान से उत्पन्न रोग अलग चीज है। यदि कोई व्यक्ति मदिरापान द्वारा रोग को इस स्थिति में ला देता है कि मात्र कुछ समय के लिए पागलपन की वह स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसने उसे दायित्व से मुक्त कर दिया होता, यदि वह अन्य किसी ढंग से कारित हुआ होता, तो वह अपराध हेतु दायित्वाधीन नहीं होता।”
(यह सिद्धांत चित्तविकृति और मत्तता के आधार पर प्रतिरक्षा के अन्तर को स्पष्ट करता है। अभियुक्त द्वारा अपने कार्य के विधिक प्रभावों का मूल्यांकन केवल चित्तविकृति के मामले में ही महत्वपूर्ण होता है।)
(3) यह जानने के लिए कि क्या अभियुक्त मदिरापान के फलस्वरूप किसी विशिष्ट आशय को सृजित करने में असमर्थ हो गया था, अन्य स्थापित तथ्यों के साथ मदिरापान के साक्ष्य को ध्यान में रखना चाहिए।
(4) यह साक्ष्य कि अभियुक्त मदिरापान किए हुए था और इस कारण वह सहज में ही तीव्र उत्तेजना के सम्मुख झुक गया, स्वतः इस बात का साक्ष्य नहीं है कि वह अपने कार्यों के स्वभाविक परिणामों को नहीं जानता था।



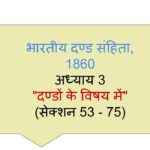

18 thoughts on “साधारण अपवाद: बाल्यपन, पागलपन, मत्तता-part 4.2”
I’m really impressed together with your writing abilities as smartly as with the structure on your blog. Is this a paid subject or did you customize it yourself? Either way keep up the nice quality writing, it’s uncommon to peer a nice blog like this one these days!
This web site is really a walk-through for all of the info you wanted about this and didn’t know who to ask. Glimpse here, and you’ll definitely discover it.
The subsequent time I read a weblog, I hope that it doesnt disappoint me as a lot as this one. I mean, I do know it was my choice to read, however I truly thought youd have something attention-grabbing to say. All I hear is a bunch of whining about something that you could repair should you werent too busy searching for attention.
Greetings from Carolina! I’m bored to tears at work so I decided to browse your blog on my iphone during lunch break. I love the info you present here and can’t wait to take a look when I get home. I’m shocked at how quick your blog loaded on my phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, wonderful site!
PlayAmo Portal Modern Gaming Site is one of the leading iGaming destinations for participants who prefer excitement, extras, and immediate transactions.
With hundreds of excellent fruit machines, poker tables, and real-time games, PlayAmo Platform delivers a elite casino adventure right from your notebook or iPhone.
New participants can receive generous launch gifts, welcome spins, and explore elite reward tiers.
Whether you explore timeless titles or the upcoming hits, PlayAmo Gaming offers everything you need for intense real cash thrills
https://gyn101.com/
gyn101.com
Good day very cool website!! Guy .. Beautiful .. Superb .. I will bookmark your website and take the feeds also…I am satisfied to seek out so many useful information right here in the submit, we want work out extra strategies on this regard, thanks for sharing.
Hmm is anyone else having problems with the pictures on this blog loading? I’m trying to find out if its a problem on my end or if it’s the blog. Any suggestions would be greatly appreciated.
What’s Happening i am new to this, I stumbled upon this I’ve found It absolutely helpful and it has aided me out loads. I hope to contribute & assist other users like its aided me. Great job.
RBVN is eh, a site. I’ve logged in. You can also. I dunno! Try it if you want! rbvn
Greetings! Very helpful advice on this article! It is the little changes that make the biggest changes. Thanks a lot for sharing!
Honestly, nilfortuneonline surprised me. The interface is clean and modern, and I’ve been having some good luck there. Give it a look-see! nilfortuneonline
Well I definitely liked studying it. This tip provided by you is very helpful for accurate planning.
Heard a lot about 639club, finally checked it out! Seems legit, easy to navigate. Gonna try my luck and see if I can hit that jackpot! Check it out for yourself: 639club
Downloaded the 7slotsapp the other day to kill some time. It’s simple, does the job. If you’re into slots and want something easy to use, give it a spin! Get the app at 7slotsapp.
Looking for a direct line? bet3333link seems reliable. Gotta have a backup plan in this game! Bookmark it, you might need it bet3333link.
Riquezaslot, sounds fancy doesn’t it? It’s slots alright, and hopefully you’ll find some riches there. Could be worth a look. Check it out: riquezaslot
51club.info seems to be the place to be! The club is pretty fun to play. The site is simple and understandable. Come joint and find 51club now.
ph828 https://www.itph828.com